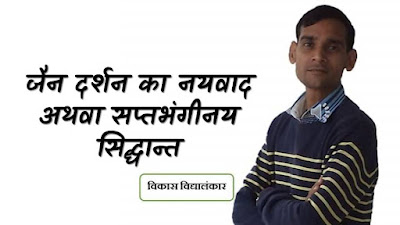|
भारतीय दर्शन |
||||
 |
| जैन दर्शन में ज्ञान के प्रकार |
जैन दर्शन में ज्ञान के प्रकार
जैन दर्शन में ज्ञान दो प्रकार का होता है-
- परोक्ष ज्ञान
तथा
- अपरोक्ष
ज्ञान।
परोक्ष ज्ञान
जो ज्ञान साधारणतया अपरोक्ष माना जाता है, वह केवल
अपेक्षाकृत अपरोक्ष है। इन्द्रियों की अपेक्षा के बगैर स्वत: प्राप्त
ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार के ज्ञान में आत्मा का पदार्थ से साक्षात्
सम्बन्ध होता है।
परोक्ष ज्ञान के प्रकार
सिद्ध सेन दिवाकर के अनुसार परोक्ष ज्ञान के प्रकार निम्नलिखित हैं-
●
स्मृतिज्ञान जिसे
पहले कभी सुना, देखा या अनुभव किया गया हो, ऐसे विषय
का यथार्थ स्मरण स्मृतिज्ञान कहलाता है।
●
प्रत्यभिज्ञा जब मनुष्य
किसी वस्तु को देखता है, तो उसे सादृश्यता का बोध होता है और वह उस वस्तु को पहचान लेता है, तब ऐसा
ज्ञान प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहलाता है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है-पहले
से जाना पहचाना।
●
तर्कज्ञान तर्क
के आधार पर अपनी युक्ति प्रस्तुत करना तर्कज्ञान होता है।
●
अनुमान ज्ञान हेतु के
द्वारा साध्य का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान ज्ञान कहलाता है।
●
आगम आप्त
पुरुषों के वचन आगम कहलाते हैं।
अपरोक्ष ज्ञान
जो ज्ञान इन्द्रियों के माध्यम से तथा मन से उत्पन्न होता है, वह अपरोक्ष
ज्ञान कहलाता है, क्योंकि इसमें आत्मा एवं वस्तुओं के बीच कोई माध्यम जैसे मन या इन्द्रियाँ
होती हैं।
अपरोक्ष ज्ञान के प्रकार
अपरोक्ष ज्ञान के दो प्रकार होते हैं-
- व्यावहारिक
ज्ञान
- पारमार्थिक
अपरोक्ष ज्ञान
व्यावहारिक ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान
में इन्द्रियों या मन के द्वारा बाह्य एवं आभ्यन्तर विषयों का ज्ञान होता है।
पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान पारमार्थिक अपरोक्ष
ज्ञान कर्म बन्धन के नष्ट होने पर प्राप्त होता है। इसमें आत्मा और ज्ञेय वस्तुओं का
सीधा सम्बन्ध होता है। राग, द्वेष, मोह, माया
में फँसे व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान तीन
प्रकार का होता है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित है
❖
अवधि
ज्ञान जब मनुष्य अपने
कर्म को अंशत: नष्ट कर लेता है, तो वह एक ऐसी
शक्ति प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा
वह अत्यन्त सूक्ष्म, दूरस्थ तथा अस्पष्ट द्रव्यों को भी जान सकता है। ऐसा तभी सम्भव है
जब मनुष्य कर्म बन्धन से छुटकारा पाने का सफल प्रयास करे। अवधि ज्ञान असीम ज्ञान है।
इसके द्वारा सीमित ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है, इसी कारण
इसे अवधि ज्ञान कहते हैं।
❖
मन:
पर्याय जब मनुष्य राग, द्वेष, मोह, माया
आदि पर विजय पा लेता है अर्थात् सभी विकारों से मुक्त हो जाता है, तब वह
अन्य व्यक्तियों के वर्तमान, भूत विचारों को
जान सकता है। इस प्रकार का ज्ञान मन: पर्याय कहलाता
है। इस प्रकार के ज्ञान से व्यक्ति दूसरे के मन को भी पढ़ने में सक्षम हो जाता है।
❖
केवल
ज्ञान ज्ञान में बाधक
सभी कर्मों के नष्ट हो जाने से आत्मा शुद्ध हो जाए अर्थात् विकार रहित हो जाए, तो अनन्त
ज्ञान प्राप्त होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होने पर सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती
है। इस प्रकार का ज्ञान केवल मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है। यह ज्ञान देश व काल
की सीमाओं से रहित होता है, इसी कारण यह ज्ञान
असीम व अनन्त होता है।
अलौकिक ज्ञान
उपरोक्त तीनों प्रकार के ज्ञान पूर्णत: अपरोक्ष
हैं। इन्हें जैन दार्शनिक अलौकिक ज्ञान भी कहते हैं। अलौकिक ज्ञान के अतिरिक्त दो प्रकार
का लौकिक ज्ञान होता है-
- मति व
- श्रुति
इनकी चर्चा इस प्रकार है-
मति ज्ञान इन्द्रियों एवं
मन से प्राप्त ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान के अन्तर्गत व्यावहारिक
अपरोक्ष ज्ञान (बाह्य) तथा अन्तर (प्रत्यक्ष, स्मृति) प्रत्यभिज्ञा
अनुमान आते हैं। मति ज्ञान दो प्रकार का होता है-
- इन्द्रियजन्य
ज्ञान तथा
- अतीन्द्रिय
ज्ञान
इन्द्रियजन्य ज्ञान में इन्द्रियों का बाह्य वस्तु से सम्पर्क होता
है। इन्द्रियजन्य ज्ञान चार प्रकार से प्राप्त होता है। उदाहरण किसी भी ध्वनि के सुनने
पर सर्वप्रथम इन्द्रियाँ संवेदन प्राप्त करती हैं, परन्तु
ज्ञात नहीं होता कि ध्वनि किसकी है। यह अवस्था 'अवग्रह' कहलाती
है। अवग्रह से केवल विषय का ग्रहण होता है। तब प्रश्न उठता है कि ध्वनि किसकी है? यह अवस्था ‘ईहा' कहलाती
है,
इसके
बाद एक निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त होता है कि ध्वनि अमुक वस्तु की है, इसे 'आवाय' कहते
हैं। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका मन में 'धारण' होता
है,
इसको ‘धारण' कहते
हैं।
श्रुति ज्ञान किसी के बताने, प्रामाणिक ग्रन्थों को सुनने अथवा आप्त वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के लिए इन्द्रिय ज्ञान का होना जरूरी है। अत: मति ज्ञान से पहले श्रुत ज्ञान आता है। श्रुति ज्ञान त्रैकालिक ज्ञान का विषय होता है। श्रुत ज्ञान अपरिणामी होता है।
------------