|
भारतीय दर्शन |
||||
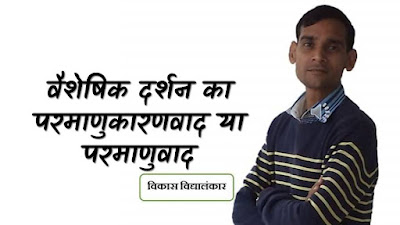 |
| वैशेषिक दर्शन का परमाणुकारणवाद या परमाणुवाद |
वैशेषिक दर्शन का परमाणुकारणवाद या परमाणुवाद
परमाणुवाद न्याय-वैशेषिक दर्शन
का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है, जिसके आधार पर
वे विश्व की सावयव वस्तुओं की उत्पत्ति एवं विनाश की व्याख्या करते हैं। चूँकि यहाँ
परमाणुओं के आधार पर भौतिक विश्व की सृष्टि एवं विनाश की व्याख्या की जाती है, इसलिए, उनका
सृष्टि सम्बन्धी सिद्धान्त परमाणुवाद कहलाता है। महर्षि गौतम परमाणु को परिभाषित करते
हुए कहते हैं कि परं वा गुटे अर्थात् जिसे और अधिक विभाजित न किया जा सके, वही परमाणु
है अतः स्पष्ट है कि परमाणु निरवयव है तथा निरवयव होने के कारण अविभाज्य है, अविभाज्य
होने के कारण नित्य है।
वैशेषिक के अनुसार, संख्यात्मक दृष्टि
से परमाणु अनन्त हैं तथा सभी परमाणु स्वभावत: निष्क्रिय
हैं। यद्यपि परमाणु नित्य हैं, किन्तु इनसे उत्पन्न
होने वाली समस्त सावयव वस्तुएँ अनित्य हैं। अत: परमाणु
संसार की समस्त सावयव वस्तुओं के उपादान का कारण है। प्रत्येक परमाणु का अपना एक विशेष
महत्त्व होता है, जो इसे अन्य परमाणुओं से अलग करता है अर्थात् कोई भी परमाणु अन्य
के समान नहीं है, चाहे वे एक ही वर्ग के क्यों न हो।
परमाणुओं के प्रकार
न्याय-वैशेषिक में चार
प्रकार के परमाणुओं को स्वीकार किया गया है-पृथ्वी, अग्नि, जल तथा
वायु के परमाणु। इन चार भूतों के अतिरिक्त आकाश एकमात्र ऐसा भूत है, जिसके
परमाणु नहीं होते, क्योंकि आकाश विभू है। आकाश चार भूतों के परमाणुओं के संयोग व वियोग
के लिए अवकाश प्रदान करता है। इन परमाणुओं में गुणात्मक तथा संख्यात्मक भेद पाया जाता
है। जैसे-वायु के परमाणु में स्पर्श का गुण पाया जाता है, किन्तु
पृथ्वी के परमाणुओं में रस, गन्ध आदि गुण
भी पाए जाते हैं, किन्तु इनमें गन्ध का गुण प्रमुख है। चूंकि सभी परमाणु सूक्ष्मतम
हैं। अत: इन्द्रियों के द्वारा उनका प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है। परमाणुओं की
सत्ता का ज्ञान अनुमान के आधार पर किया जाता है। आकाश नामक भूत का ज्ञान भी अनुमान
पर ही आधारित है।
वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धि के तर्क
वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धि के लिए निम्नलिखित तर्क दिए गए
हैं-
●
वैशेषिक के मतानुसार जितने भी सावयव पदार्थ
हैं,
वे
अनित्य हैं। यदि इन सावयव पदार्थों का विभाजन किया जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इनका
और अधिक विभाजन सम्भव नहीं होगा। यदि हम इस विभाजन की प्रक्रिया को स्थिर नहीं जानेगे
तो
'अनावस्था
दोष'
उत्पन्न
हो जाएगा। अत: इस दोष से बचने के लिए निरवयव, अविभाज्य
तथा सूक्ष्मतम तत्त्व के रूप में इन परमाणुओं का मानना आवश्यक है।
●
वैशेषिक के मतानुसार, जिस प्रकार
हम बड़े परिमाण की ओर बढ़ते-बढ़ते आकाश तक
पहँचते हैं जिससे बड़ा कोई परिमाण नहीं है, ठीक उसी प्रकार
सबसे छोटा परिमाण भी होना चाहिए, क्योंकि संसार
में प्रत्येक वस्तु की एक विरोधी वस्तु विद्यमान है। अतः परमाणु ही वह सबसे छोटा परिमाण
है।
●
न्याय-वैशेषिक
मतानुसार, परमाणु स्वभावतः निष्क्रिय हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उभरकर
सामने आता है कि निष्क्रिय परमाणुओं से जगत की रचना क्यों और कैसे तथा किसके द्वारा
की गई है?
●
न्याय-वैशेषिक
मतानुसार, जीवों को उनके कर्मों का उचित फल प्रदान करने के लिए ईश्वर द्वारा
इस जगत की रचना निष्क्रिय परमाणुओं में गति को उत्पन्न करके की है। इस क्रम में सर्वप्रथम
ईश्वर दो परमाणुओं को आपस में मिलाकर द्विअणु की रचना के पश्चात् तीन द्विअणुओं के
संयोग से एक त्रयणुक का निर्माण करता है। यह त्रयणुक सृष्टि का सूक्ष्मतम दृष्टिगोचर
होने वाला द्रव्य है, परमाणुओं का यह संयोग क्रम चलता रहता है और इस प्रकार सृष्टि निर्माण
की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।
परमाणुवाद की मुख्य विशेषताएँ
न्याय-वैशेषिक परमाणुवाद
की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
●
न्याय-वैशेषिक
परमाणुवाद, ईश्वरवाद तथा अनीश्वरवाद का समन्वय करता है। ईश्वरवाद ईश्वर को जगत
का कारण मानता है तथा अनीश्वरवाद भौतिक तत्त्वों या परमाणुओं के आधार पर जगत की उत्पत्ति
एवं विकास की व्याख्या करता है। न्याय-वैशेषिक दर्शन
में परमाणुओं के संयोग से जगत की उत्पत्ति की बात की गई है, परन्तु
साथ में यह भी कहा गया है कि यह सृष्टि ईश्वर की इच्छा से स्वयं ईश्वर द्वारा की गई
है।
●
न्याय-वैशेषिक
का यह परमाणुवाद केवल अनित्य या सावयव जगत की उत्पत्ति एवं विनाश की व्याख्या करता
है। यहाँ देश-काल, मन तथा आत्मा आदि नित्य द्रव्यों की व्याख्या परमाणुओं के आधार पर
नहीं की गई है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद की उक्त विवेचना की गई है, जिसके
विरुद्ध अद्वैत के प्रतिपादक शंकर ने निम्न आक्षेप लगाए हैं-
❖
यदि परमाणु स्वभावतः निष्क्रिय है, तो ऐसी
स्थिति में सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या नहीं हो पाती।
❖
यदि परमाणुओं को सदैव सक्रिय माना जाए तो
ऐसी स्थिति में सदैव सृष्टि ही होती रहेगी, विनाश की व्याख्या
नहीं हो पाएगी।
❖
यदि परमाणुओं को निष्क्रिय एवं सक्रिय दोनों
माना जाए तो आत्मविरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है और यदि परमाणुओं को न निष्क्रिय
माना जाए, न सक्रिय माना जाए तो ऐसी स्थिति अकल्पनीय होगी।
❖
परमाणु नित्य नहीं हो सकते क्योंकि ये भौतिक
वस्तुओं की मूल इकाई हैं। ये निरवयव भी नहीं हो सकते, क्योंकि
इनकी वस्तुगत सत्ता है।
❖
परमाणुवाद में ईश्वर की कल्पना बाह्य आरोपित
है।
--------------





