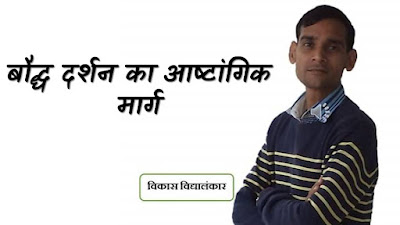|
भारतीय दर्शन |
||||
 |
| बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद (नैरात्मवाद) |
बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद (नैरात्मवाद)
चार्वाक को छोड़कर अन्य भारतीय दर्शनों में आत्मा को नित्य, शाश्वत, अमर तत्त्व
के रूप में स्वीकार किया गया है। बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद का सिद्धान्त आत्मा सम्बन्धी
परम्परागत मतों से भिन्नता एवं विपरीतता को दर्शाता है अनात्मवाद बौद्ध दर्शन के केन्द्रीय
सिद्धान्त प्रतीत्यसमुत्पाद की ही तार्किक परिणति है।
अनात्मवाद के अनुसार आत्मा नित्य, शाश्वत, अमर नहीं
है,
बल्कि
वह भी सांसारिक वस्तुओं की भाँति निरन्तर परिवर्तनशील है। यदि अनात्मवाद को संकीर्ण
अर्थ में लिया जाए तो इसका आशय है ‘आत्मा के अस्तित्व
का खण्डन' या उसकी 'अस्तित्वहीनता'। ऐसी
स्थिति में यह सिद्धान्त उच्छेदवाद के समतुल्य होगा। ऐसा मानने पर मध्यम प्रतिपदा के
उनके सिद्धान्त का खण्डन होगा। अत: अनात्मवाद का
यह अर्थ स्वीकार्य नहीं है।
अनात्मवाद का आशय यह नहीं है कि ‘आत्मा
नहीं है'। अनात्मवाद का आशय है कि 'वैसी
आत्मा नहीं है' जिसका उल्लेख उपनिषद् दर्शन में मिलता है। उल्लेखनीय है कि उपनिषद्
दर्शन में आत्मा को नित्य, अजर, अमर, अविनाशी
तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। बुद्ध के अनुसार, नित्य
आत्मा में विश्वास करना उसी प्रकार हास्यास्पद है, जिस प्रकार
कल्पित सुन्दर रमणी के प्रति आसक्ति रखना हास्यास्पद है।
बौद्ध धर्म उपदेशक नागसेन मिलिन्द प्रश्न में आत्मा के स्वरूप को
स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार धुरी, चक्के, लगाम, घोड़े
आदि के संघात को रथ कहा जाता है, उसी प्रकार पाँच
स्कन्धों-रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार
और चेतना का संघात ही आत्मा है। ये पाँचों स्कन्ध अनित्य हैं। अत: आत्मा
भी अनित्य है अर्थात् स्कन्धों के निरन्तर परिवर्तनशील होने के कारण आत्मा भी निरन्तर
परिवर्तनशील है।
बौद्ध के अनात्मवाद के समर्थन में तर्क
बौद्ध के अनात्मवाद के समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते
हैं-
●
शरीर का संचालन आत्मा के द्वारा होता है।
यदि आत्मा को स्थायी माना जाए तो शरीर के संचालन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अत: आत्मा
को परिवर्तनशील मानना अनिवार्य है। इस तर्क को स्वीकार करने में समस्या है, क्योंकि
संचालन, संचालनकर्ता के संकल्प पर आधारित होता है।
●
अब यदि संचालनकर्ता स्थिर नहीं है, तो उसके
संकल्प में भी परिवर्तन होता रहेगा, फलत: क्रियाएँ
भी बदल जाएँगी। सफल संचालन के लिए संचालनकर्ता के संकल्प को स्थिर मानना आवश्यक है।
यह तभी सम्भव हो सकता है, जब संचालनकर्ता
स्वयं स्थिर हो।
●
यदि आत्मा नित्य, शाश्वत, अमर एवं
अपरिवर्तनशील है, तो ऐसी स्थिति में वह कर्मों का सम्पादन नहीं कर सकती। अत: वह किसी
फल के लिए भी उत्तरदायी नहीं है। अत: उसे परिवर्तनशील
माने बिना कर्म नियम की संगत व्याख्या नहीं हो सकती। किन्तु इस तर्क को लेकर समस्या
यह है कि यदि आत्मा निरन्तर परिवतर्नशील है, तो ऐसी स्थिति
में कर्म नियम की संगत व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि
तब कर्म कोई करेगा और फल किसी और को मिलेगा।
●
बुद्ध ने स्वयं कहा है कि संचित कर्मों
का फल भोग करने के लिए पुनर्जन्म होता है। बुद्ध की यह बात उनके अनात्मवाद के साथ संगत
नहीं ठहरती, क्योंकि यदि कोई नित्य आत्मा नहीं है तो फल भोग कौन करता है। अत: कर्म
नियम सिद्धान्त की संगत व्याख्या करने के लिए नित्य आत्मा को स्वीकार करना अनिवार्य
है।
●
यदि आत्मा नित्य है, तो वह
न तो जन्म ले सकती है और न ही मर सकती है। नित्य आत्मा को मानने पर पुनर्जन्म की संगत
व्याख्या नहीं की जा सकती है, किन्तु इस तर्क
को लेकर समस्या यह है कि यदि आत्मा परिवर्तनशील है, तो यह
कैसे कहा जा सकता है कि जिसका जन्म हुआ है, वह वही है। यह
कैसे कहा जा सकता है कि जिसकी मृत्यु हुई है, वह वही
है जिसने जन्म लिया था? यह तभी कहा जा सकता है, जब आत्मा को नित्य
माना जाए।
●
यदि आत्मा नित्य है तो उसकी दो स्थितियाँ
हो सकती हैं-शुद्ध आत्मा तथा अशुद्ध आत्मा। अब यदि आत्मा शुद्ध है तथा अपरिवर्तनशील
है,
तो
वह कभी बन्धन में नहीं पड़ सकती और यदि आत्मा अशुद्ध है अर्थात् बन्धन में है, तो अपरिवर्तनशील
होने के कारण कभी शुद्ध नहीं हो सकती।
●
अत: आत्मा
को नित्य तथा शाश्वत मानने पर बन्धन और मोक्ष की तर्कसंगत व्याख्या नहीं हो सकती। किन्तु
इस तर्क को लेकर समस्या यह है कि यदि आत्मा परिवर्तनशील है, तो ऐसी
स्थिति में जो आत्मा मोक्ष के लिए प्रयास करेगी, उसे मोक्ष
न मिलकर किसी और को मोक्ष मिलेगा, जो कर्म नियम
के साथ संगत नहीं है। संगत यह है कि जो कर्म करे उसे ही उसका फल भी प्राप्त हो और सम्भव
है जब एक नित्य आत्मा को स्वीकार किया जाए।
●
एक विशेष सन्दर्भ में वर्तमान मनोविज्ञान
भी आत्मा को परिवर्तनशील मानता है, उसके अनुसार व्यक्तित्व
भौतिक एवं मानसिक घटकों का गत्यात्मक संगठन है। किन्तु इस तर्क को लेकर समस्या यह है
कि यदि व्यक्तित्व भौतिक और मानसिक घटकों का एक गत्यात्मक संगठन है अर्थात् हम में
सब कुछ परिवर्तनशील है तो हमें कैसे याद आता है कि वह तो वही व्यक्ति है? हमारी
स्मृति का आधार क्या है? यदि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो स्मृति
को भी परिवर्तनशील मानना होगा।
●
ऐसी स्थिति में हमारे भीतर विद्यमान ज्ञान
को ज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज्ञान
वह है जिसमें स्थायित्व हो, साथ ही जो निरन्तर
विकसित और परिमार्जित हो। अत: ज्ञान के स्थायित्व, विकास
और परिमार्जन के लिए स्मृति को अपरिवर्तनशील मानना होगा। स्मृति अपने आप नहीं रह सकती।
अत:
इसके
आश्रय के रूप में नित्य आत्मा को मानना अनिवार्य है, क्योंकि
यदि आधार ही परिवर्तनशील है, तो स्मृति भी
परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकती।
अत: उपरोक्त के आधार पर निष्कर्षत: कहा जा
सकता है कि आत्मा की नित्यता तथा परिवर्तनशीलता दोनों के सम्बन्ध में प्रबल तर्क है।
तर्कों के आधार पर न तो आत्मा की नित्यता को सिद्ध किया जा सकता है और न ही अनित्यता
को। अत: श्रेयस्कर यही होगा कि इस विवाद में न पड़ते हुए मौन का अवलम्बन
किया जाए।
प्रतीत्यसमुत्पाद की अनात्मवाद के पक्ष में युक्ति
बुद्ध के उपदेश के समय समाज में उपनिषद् दर्शन का प्रचलन था। जिसकी मान्यता थी कि मानव के भीतर एक महत्त्वूपर्ण तत्त्व आत्मा है। इस आत्मा का जन्म नहीं होता, बल्कि वह शरीर धारण करती है। यह आत्मा नित्य, अजर, अमर तथा अविनाशी है। उपनिषद् दर्शन का यह विचार बौद्ध दर्शन में अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि बुद्ध की मान्यता थी कि ब्रह्माण्ड में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है जो नित्य या अपरिवर्तनशील हो, इसलिए मानव के भीतर नित्य आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। मानव पाँच स्कन्धों का एक संघात है। ये पाँच स्कन्ध निम्नलिखित हैं-
●
रूप शरीर का आकार
एवं अन्य शारीरिक धर्म।
●
वेदना सारे रूप मिलकर
वेदना उत्पन्न करते हैं।
●
संज्ञा ज्ञान प्राप्त
करने का अनुभव।
●
संस्कार अनुभव से जो
तत्त्व उत्पन्न होता है।
●
चेतना संस्कारों की
समग्रता से चेतना का निर्माण होता है। यहाँ समग्रता से तात्पर्य समुच्चय से नहीं, बल्कि
निरन्तर प्रवाह से है।
बुद्ध के अनुसार, उपरोक्त पाँचों
स्कन्धों में से कोई ऐसा नहीं है जो नष्ट नहीं होता हो। आशय यह है कि सभी स्कन्ध नष्ट
होते हैं, किन्तु पूर्णरूप से नहीं बल्कि एक तत्त्व नष्ट होते-होते
अन्य में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि मानव इन्हीं पाँच स्कन्धों का एक बड़ा संघात
है,
अत: मानव
में कुछ भी ऐसा नहीं जो नित्य या अपरिवर्तनशील हो, इसे ही
अनात्मवाद कहा जाता है।
बुद्ध के मतानुसार आत्मा अनित्य है, क्योंकि
यह निरन्तर परिवर्तनशील उपरोक्त पाँच संघातों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार
नदी में जल की बूंदें निरन्तर परिवर्तित होती रहती हैं, फिर भी
उनमें एकमयता रहती है, वैसे ही आत्मा के विज्ञान (चेतना) के निरन्तर
बदलते रहने पर भी उसमें एकमयता रहती है। ह्यूम के आत्मा सम्बन्धी विचार में बुद्ध के
आत्मा सम्बन्धी विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, क्योंकि
ह्यूम ने भी आत्मा को 'संवेदना का समूह' कहा है जिसमें
निरन्तर परिवर्तन होता रहता है।
बुद्ध द्वारा प्रस्तुत अनात्मवाद के समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत
किए जा सकते हैं-
●
यदि आत्मा को परिवर्तनशील न माना जाए, तो शरीर
के संचालन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
●
कर्मों का सम्पादन करने के लिए आत्मा को
परिवर्तनशील मानना अनिवार्य है।
●
पुनर्जन्म की व्याख्या करने के लिए आत्मा
को परिवर्तनशील मानना अनिवार्य है, क्योंकि स्थिर
आत्मा न तो शरीर धारण कर सकती है और न ही त्याग सकती है।
● वर्तमान मनोविज्ञान के अनुसार आत्मा भौतिक तथा मानसिक घटकों; जैसे- बुद्धि, स्वभाव, शरीर के विभिन्न रसायनों, आनुवंशिक तत्त्वों एवं विभिन्न परिस्थिति से प्राप्त गतिशील तत्त्वों का संघटन मात्र है।
-------------